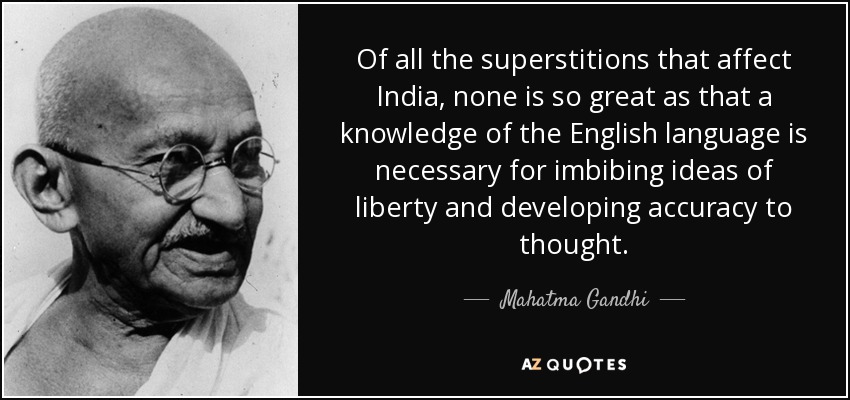 |
|---|
| गांधीजी ने कहा है या नहीं, ये नहीं पता… अच्छा लगा तो डाल दी यहाँ 😁 |
पिछले लेख में मैंने बोला था कि एक वैकल्पिक मातृभाषा-केंद्रित प्रणाली के बारे में लिखूंगा, मगर लिखते लिखते ऐसा लगा कि विकल्प पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि विगत समय में इस मुद्दे को लेकर क्या क्या हुआ है भारत में; भारत में भाषा का संक्षिप्त इतिहास। ऐसा नहीं है कि आजतक कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई; चर्चा तो दूर की बात दंगे तक हो चुके हैं। आत्महत्याएं तक हुई हैं मातृभाषा को लेकर, तो आइये जानते हैं कि आज का सरकारी तंत्र यहाँ तक पहुँचा कैसे।
भाषानीति : स्वतंत्रता के पहले
भाषा सदा से राजनीति का एक अभिन्न अंग रही हैं। मौर्यवंश के समय में ब्राह्मी से लेकर प्राकृत-हिंदी-संस्कृत के आपसी टकराव और दिल्ली सल्तनत के समय से उर्दू-फ़ारसी के उदय तक, भाषा हमेशा से साम्राज्यों/संस्कृतियों की पैठ बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम रही है। भाषा और संस्कृति का आपसी जुड़ाव किस हद तक जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं लॉर्ड थॉमस मैकॉले और तत्कालीन अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम में उनकी भूमिका को मानता हूँ।
१८३५(1835) से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा/साहित्य पर किये जा रहे खर्चों में ऐसी पाठशालाएँ-विश्वविद्यालय भी सम्मिलित थीं जिनमें “देशज” भाषाओं(संस्कृत और अरबी-फ़ारसी) में लिखे हुए साहित्य की पढ़ाई होती थी। देशज भाषाएँ ही पढ़ाई का माध्यम हुआ करती थीं। इंग्लैंड में बैठी हुई अंग्रेज़ सरकार द्वारा प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके भारतीय साम्राज्य में साहित्य को बढ़ावा देने एवं पढ़े-लिखे भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जाएँ।
१८३५ में इससे सम्बन्धित अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम को मंज़ूरी दी गई, जिसमें प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अरबी-संस्कृत भाषाओं में किये जा रहे अपने प्रकाशनों पर रोक लगाए और केवल अंग्रेज़ी भाषा में ही पाठ्य सामग्री प्रकाशित करे। इसके अलावा “देशज” भाषा-माध्यम में चल रही पाठशालाओं-विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले पैसे(अध्यापकगण एवं छात्रगणों को दिया जाने वाला मानदेय(Salary/Stipend)) पर रोक लगाने जैसे प्रावधान भी लाए गए।
चार साल बाद ही हालांकि इस अधिनियम को आंशिक रूप से वापिस ले लिया गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये थी कि इन बदलावों के पीछे की इच्छा क्या थी। इस फैसले को लेकर अंग्रेज़ संसद के दो धड़ों, “अपरिवर्तनवादी”(Conservatives) और “सुधारवादी”(Reformists/Anglicists) में टकराव था। इससे पहले अंग्रेज़ सरकार की नीति थी कि भारतीय भाषाओं में ही अनुवाद करके पाश्चात्य सामग्री पढ़ाई जाए, लेकिन लम्बे समय से “सुधारवादी” (शब्द से मेरे अपने मतभेद हैं, लेकिन अनुवाद यही है Reformists का) धड़े की मांग थी कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करके अंग्रेज़ी शिक्षा माध्यम में पढ़ाई हो।
लॉर्ड थॉमस मैकॉले : भाषा के उपयोग
“सुधारवादी” धड़े के अगुवा और शिक्षण समिति के भावी अध्यक्ष थॉमस मैकॉले ने इस बहस के अंत तक अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया। १८३३(1833) के समय से ही मैकॉले अंग्रेज़ी शिक्षा का समर्थन करते आ रहे थे; उनका मानना था कि अंग्रेज़ी संस्कृति भारतीय संस्कृति से कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट है और भारतीय समाज को “शिक्षित” बनाना उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। उनके बयान देखेंगे तो “उत्कृष्टता” वाली चीज़ आपको आराम से नज़र आ जाएगी :
- “… that it is impossible for us, with our limited means, to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.” (विस्तार में पढ़ें : अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम)
सामाजिक अभियांत्रिकी(Social Engineering) और भाषा के संबंध का मुझे इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिला। “educate”, “refine”, “enrich”, “knowledge”, ये शब्द आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं में इस बयान की बारीकी है, और सार है एक समाज को बदलने का। बाकी तो आप देख ही सकते हैं साफ़ लिखा हुआ, उसको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है।
अपने-आप में १८३५(1835) के अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम की कुछ ज़्यादा महत्ता नहीं है, लेकिन उसकी बहस में आपको दिख जाएगा कि भाषा कितना शक्तिशाली माध्यम है समाज बदलने का। भारत में भाषा की गाथा के इस अध्याय को यहाँ लिखना इसीलिए जरूरी लगा; भाषा और संस्कृति को इस तरीके से जोड़ने वाले ऐतिहासिक उदाहरण कम ही लगते हैं मुझे। अब जब हमने देख लिया है कि भाषा और समाज का संबंध कितना गहरा है, चलते हैं भाषानीति के अपेक्षाकृत नए इतिहास की ओर, स्वतंत्रता के बाद।
भाषानीति : स्वतंत्रता के बाद
अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद भारत के नेता भारत के सभी क्षेत्रों को एक करना चाहते थे, और उनका ये मानना था कि इसके लिए पूरे देश को एक भाषा में जोड़ना आवश्यक है। महात्मा गांधी के हिसाब से पूरे देश में किसी भाषा के स्वीकार किये जाने के लिए उसमें पाँच विशेषताएँ होना आवश्यक था :
— सरकारी अफसर उसे आसानी से सीख पाएँ
— वो भाषा पूरे देश के धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक संवाद का माध्यम बनने में समर्थ हो
— वो देश के सर्वाधिक नागरिकों के बोलचाल की भाषा हो
— पूरा देश उसको आसानी से सीख पाए
— इस भाषा को चुनने में अस्थायी फायदों को न जाए
पूरे देश में हिंदी का प्रभुत्व नहीं था, लेकिन शुरू से हिंदी ही इसके लिए पहली पसंद थी हिंदी को देश में सबसे ज़्यादा लोग बोलते थे(हैं) और मराठी जैसी अन्य भाषाएँ भी हिंदी से ज़्यादा अलग नहीं थी। द्रविड़ भाषाएं हिंदी से ज़्यादा संबंध नहीं रखती थीं, मगर दोनों में संस्कृत भाषा का प्रबल प्रभाव था। शायद इसी कारण हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा चुना गया, लेकिन इस आश्वासन के साथ कि हिंदी को कभी गैर-हिंदी क्षेत्रों पर नहीं थोपा जाएगा।
भाषाई दंगे और त्रि-भाषा सूत्र
हिंदी को आधिकारिक भाषा चुने जाने के समय (1950 के आसपास) पर दक्षिण भारत के राज्यों ने यह दलील दी कि अंग्रेज़-शासन के समय से वहाँ अंग्रेज़ी का प्रयोग हो रहा है, अतः उनको हिंदी भाषा में कामकाज करने के लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। तय हुआ कि 15 साल बाद सरकारी कामकाज पूरी तरह हिंदी में किया जाने लगेगा।
1965 में जब इस बदलाव को लागू करने की बात आई तो मुख्यतः तमिलनाडु में इसका हिंसक विरोध हुआ। आंदोलन के अंत में केंद्र सरकार को मजबूर होकर अंग्रेज़ी को भी सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर रखना पड़ा। 1968 में त्रि-भाषा सूत्र को लागू किया गया, जिसमें प्रावधान था कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेज़ी व एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी, और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में राज्य की मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी।
त्रि-भाषा सूत्र कागज़ों में काफी सही लगा था, पर कागज़ों से हटकर इसका ढंग से कभी पालन नहीं हुआ। उत्तर भारतीय राज्यों ने इसका कुछ समय पालन किया और फिर ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया। उत्तर भारतीय राज्यों की बेरुखी देखकर तमिलनाडु में भी फिर से आंदोलन हुआ और अंततः वहाँ से हिंदी भाषा को पूरी तरह हटा दिया गया। कई राज्यों में यह सूत्र आज भी लागू है, जैसे आंध्र-प्रदेश, केरल, उड़ीसा आदि। हिंदी भाषी राज्यों में संस्कृत प्रयोग करते हैं कई जगह, लेकिन इसको त्रि-भाषा सूत्र से बचने का रास्ता ज़्यादा समझा जाता है।
भाषानीति : आज की स्थिति
1968 के बाद 1986 और बाद की शिक्षा नीतियों में त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने की बात करी गई, और बात करके छोड़ दी गई। भारतीय भाषाओं के इस आपस के द्वंद्व के कारण अंग्रेज़ी का उदय जारी रहा, और आज निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़कर अंग्रेज़ी उच्च वर्ग के उत्थान और सत्ता का माध्यम बन बैठी है।
ये मैं नहीं, 2019 की शिक्षा नीति का प्रारूप कह रहा है।
2019 के शिक्षा नीति प्रारूप में भाषाओं को कई पन्ने समर्पित हैं, और कई चीज़ों को अभूतपूर्व ढंग से कहा गया है। मेरे अपने कुछ मतभेद हैं, लेकिन पुरानी नीतियों से ये तब भी कहीं बेहतर है भाषा के सन्दर्भ में।अगले लेख में इस पर विस्तार से।
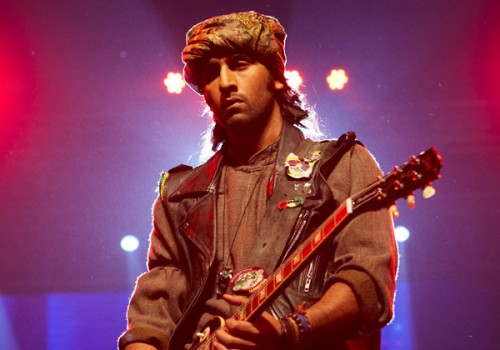
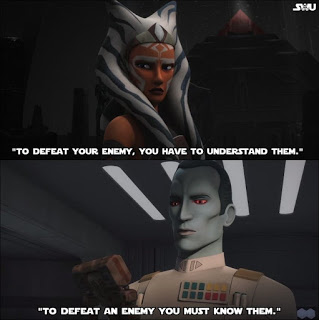
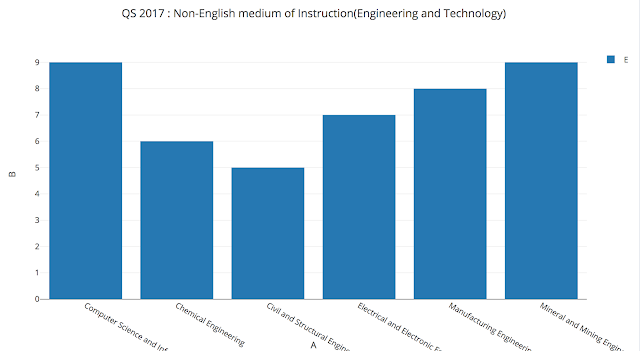
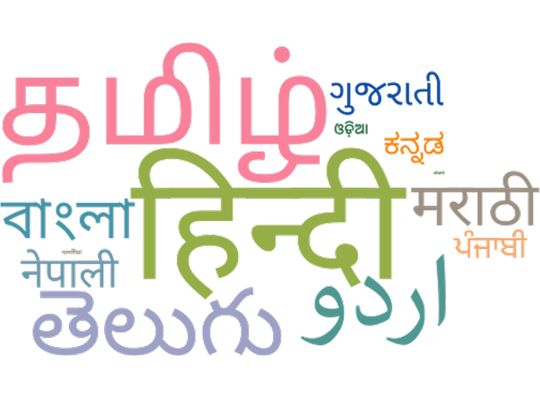
एक टिप्पणी छोड़ें